तृतीय अध्याय
अंतरिक्ष की अनेकता
आपः नामक अंतरिक्ष
लोकत्रयी में अंतरिक्ष
सप्तप्राणाः
सप्त अपानाः
सप्त व्यानाः
सप्तलोकों की परिकल्पना
आपः नामक अंतरिक्ष
गोपथ-ब्राह्मण का सृष्टि-वर्णन
वेदों और व्याहृतियों का मनोविज्ञान
विश्वेदेवाः
निष्कर्ष
तृतीय अध्याय
अन्तरिक्ष की अनेकता
पिछले अध्याय में हमें अन्तरिक्ष की अवधारणा के विषय में दो सम्भावनाओं के संकेत मिले । प्रथम तो हमें यह प्रतीत हुआ कि अन्तरिक्ष कोई व्यापक अन्तश्चेतना है । दूसरे, हमने उसे व्यष्टिगत अन्तश्चेतना के रूप में देखा जिसे उस लोक में परिणत करने की कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ वेद-मन्त्रों में अनेक अन्तरिक्षों का उल्लेख भी मिलता है जिससे अन्तरिक्ष की अवधारणा में एक नई जटिलता आ जाती है। प्रस्तुत अध्याय में इसी समस्या पर विचार किया जाएगा।
आपः नामक अन्तरिक्ष
यों तो अन्तरिक्ष की अनेकता का बोध उसके निघण्टुगत आपः नाम में ही निहित है, क्योंकि यह शब्द न केवल वैदिक वाङ्मय में, अपितु लौकिक संस्कृत में भी, सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत में आपः जलवाचक है और निघण्टु के १०१ जलनामानि में भी इसको गिनाया गया है। इसीलिये, वेद में, न केवल आपः को, अपितु अन्य जल-नामों को भी प्रायः जलवाचक ही समझा जाता है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि निघण्टु के १०१ जल नामों में सत्यम्,
ऋतम्, ऋतस्य योनिः, सत्, पूर्णम्, भूतम्, भुवनम्, भविष्यत् तथा महत् जैसे शब्दों के साथ ही कुछ अन्तरिक्षनाम तथा कुछ असुरनाम (अहि, शंबर) भी समाविष्ट हैं । अतः विवश होकर सोचना पड़ता है कि इन जल नामों की पृष्ठभूमि में कोई प्रतीकवाद तो नहीं है ?
ब्राह्मण-ग्रन्थों में आपः के कुछ समीकरणों को देखकर भी ऐसा ही लगता है। उदाहरण के लिए, शतपथब्राह्मण में आपः और वाक् का समीकरण विशेषरूप से उल्लेखनीय है ।१ सामान्यतः वाक् का अर्थ बोलने की शक्ति, वाणी अथवा शब्द होता है, परन्तु वैदिक वाङ्मय में वाक् वह शक्ति है जो सृष्टि करती है।२ इसी प्रकार, आपः भी सृष्टि करने वाली शक्ति के रूप में जाने जाते हैं।३ अतः यह कहना अनुचित न होगा कि वाक् नामक शक्ति का द्योतक ही "आपः' नामक अन्तरिक्ष है। इसीलिए, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ४.११.१.११ "वागित्यंतरिक्षम्" की घोषणा करता है और आपः अन्तरिक्षनामों में परिगणित है ।
अतएव, जब वाक् को सभी लोकों में "वितत" हुआ माना जाता है४, तो वेद-मन्त्रों में उल्लिखित अनेक अन्तरिक्ष भी उक्त वाक्-रूप अन्तरिक्ष के रूपान्तर माने जा सकते हैं । इसीलिए लोकों को वाक्
----
१.सा वाक् इदं सर्वमाप्नोद् यदिदं किं च। यदाप्नोत्तस्मादापः। माश.६.१.१.९ २.प्रजापतिर्वा इदमासीत् तस्य वाक् द्वितीया आसीत्.....सा इमाः प्रजाः असृजत् काठ.१२.५; २७.१; क ४२.१
३.आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास। ता अकामयन्त कथं नु प्रजायेमहीति। -माश ११.१.६.१
४.वाग् वा इयं वितता यदिमे लोकाः जैब्रा.२.३८९; २.२५३; २६४
५.तु अन्तरिक्षाणि ऋ.१०.६५.४; ८.६.१५; ८.१२.२४ ; अथ.२०.९४.८
की व्याहृतियां कहा जाता है - एता वै व्याहृतयः इमे लोकाः (तैआ २.२.४.३) और अन्तरिक्ष के रूपान्तरों को ही भूः, भुवः आदि कहा जाता है (तैआ ७.५.१; तैउ १.५.१; जैब्रा १.३६४; माश १२.३.४.७; गोब्रा १.५.१५ ) इसका अर्थ है कि वाक्, आपः अथवा अन्तरिक्षनामक चेतना-शक्ति के मूल रूप को ही वह अनारम्भणं अन्तरिक्षम्" कहा जा सकता है जो सभी देवों का आयतन है। इसी को "अयं वाव समुद्रो अनारम्भणो यदिदमन्तरिक्षम् (तां २०.१४३, जैब्रा १.१६५) कहकर याद किया जाता है । दूसरे शब्दों में, वाक्, आपः अथवा अन्तरिक्षम् नामक चेतना-शक्ति का मूल रूप ही वह अनारम्भण समुद्र है जिससे उद्भूत अनेक चेतना-धाराओं को अनेक व्याहृतियां, अनेक लोक, अनेक आपः अथवा अनेक अन्तरिक्षों के रूप में कल्पित किया गया है । इस प्रसंग में, इन सभी नामों के संदर्भ में, यह भी उल्लेखनीय है कि “समुद्र' शब्द भी अन्तरिक्षनामों में परिगणित है और अन्तरिक्ष को प्रजापति की महिमा आपः भी कहा जाता है। यह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निघण्टु के अन्तरिक्षनामों में 'आपः' की भी गणना की गई है। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के निम्नलिखित दो मन्त्र भी स्मरणीय हैं जिनमें सहस्राक्षरा वाक् परमव्योम में सलिलों का तक्षण करती हुई, नवपदों तक गति करती है और उसके समुद्र जिस सलिल का क्षरण करते हैं उससे चारों प्रदिशाएं और समस्त विश्व जीवन धारण करता है-
गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी,
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ।
तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः,
ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति । ऋ.१.१६४.४१-४२
-----
१.काठसं.४५.१२
संयोगवश, यहां एक अन्य अन्तरिक्षनाम व्योम भी आ गया। यह वही परमव्योम है जिसमें वह विराज् वाक् रहती है जिसके उठने पर सभी यज्ञ उठ पड़ते हैं और जिस के च्युत होने पर सभी यज्ञ च्युत हो जाते हैं, जबकि उसके प्रसव-रूप व्रत में यक्ष गतिशील हो जाता है ।१ यह यक्ष वही ब्रह्मविदों का ब्रह्म-रूप यक्ष है जो आत्मा
से युक्त होकर हिरण्ययकोश के ज्योतिर्मण्डित स्वर्ग में विराजमान रहता है।२ अतः इस विराज् वाक् को उसी ब्रह्म की शक्ति कह सकते है जिसके प्रसव से वह (शक्तिमान) गतिशील हो जाता है । इसीलिए, उक्त रहस्यमय परमव्योम को स्वयं ब्रह्मा ही कहा गया है -
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम (ऋ.१.१६४.३५; अथ ९.१५.१४) । यही वह वाक् है जिससे यज्ञ संतत हुआ कहा जाता है अथवा जिसको यज्ञ का रूप कहा जाता है । इसी वाक् को पुनः "विराट् वै यज्ञः - माश १.१.१.२२; २.३.१.१८; ४.४.५.१९) कहा गया है। यह परमव्योम अक्षर है जिसमें सभी विश्वेदेवा अधिष्ठित माने जाते हैं।४
ब्रह्म के इस परमव्योम के अतिरिक्त वेद में एक व्योम का उल्लेख भी मिलता है जिसमें आसीन “व्योम-सद्”५ हंस को आत्मा माना जा सकता है। अतः परमव्योम को ब्रह्माण्डीय उरु अन्तरिक्ष
-----
१.यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्।
यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराडृषयः परमे व्योमन्।।-अथ.८.९.८
२.तस्मिन् यक्षं आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः। -अथ.१०.२.३२
३.वाचा यज्ञः संततः, मैसं १.११.६ तु.वाग् वै यज्ञः ऐब्रा.५.२४; माश १.१.२.२; ३.१.३.२७; २.२.३
४.अथ.९.१५.१८
५.हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर् दुरोणसत्,
नृषद् वरसद् ऋतसद् व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् तै ४.१.५; ऋ.४.४०.५; मै.२.६.१२; काठक १५.८; काठक १६.८; का ११.७.४
कह सकते हैं जिससे अन्य अन्तरिक्षाणि अधवा लोकों का प्रादुर्भाव होता है। यह व्योम ही वह स्वर्ग है जिस पर अधिरोहण करके आत्मा उस ब्रह्माण्डीय परमव्योम में पहुंचता है जिसे "उत्तमं नाकं" कहा जाता है -
श्राम्यतः पचतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमधि रोहयैनम् ।
येन रोहात् परमापद्य यद् वय उत्तमं नाकं परमं व्योम् ।। -अथ ११.१.३० इस मन्त्र में स्वर्गारोहण के लिए जिस पंथ का ज्ञान आवश्यक माना गया है, वह वही यज्ञ है जो मनुष्य-व्यक्तित्व-रूपी उस वेदी पर होता है जिसे ऋत के द्वारा निर्मित तथा मन के द्वारा प्रस्तुत “ब्रह्मौदन की वेदी” कहा जाता है ।१ यह अद्भुत यज्ञ है जिसमें उर्जा का भाग निहित है, जिससे आपः का आभरण भी किया जाता है । इस यज्ञ के लिए गातुवित्, नाथवित्, प्रजावित्, पशुवित् और वीरवित् होने की कामना की जाती है -
ऊर्जो भागो निहितो यः परा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरैताः ।
अयं यज्ञो गातुविन्नाथवित् प्रजा विदुग्रः पशुविद् वीरविद् वो अस्तु।।-अथ ११.१.१५
यह यज्ञ निस्संदेह आध्यात्मिक यज्ञ है। गातु नामक देवयान के प्रसंग से वह 'गातुविद् ' है। विश्वनाथ (ईश्वर) के सम्बन्ध से वह "नाथवित्' है। श्रेष्ठ बुद्धि-रूप प्रजा को जन्म देने से उसे “प्रजावित्', सत्यद्रष्टा प्राणों रूपी पशुओं को उत्पन्न करने से ही वह “पशुवित्”
--------------
१.ऋतेन तष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदनस्य विहिता वेदिरग्रे ।
अंसद्रीं शुद्धामुप धेहि नारि तत्रोदनं सादय देवानाम् ।। -अथ ११.१.२३
तथा अहंकार-रूप वृत्र-वध में सहायक वीर प्राणों को उद्धृत करने के कारण वही 'वीरवित्" भी कहा जाता है। ये वीर प्राण ही उस अदिति के पुत्र आदित्य हैं जिनके उत्पन्न करने के लिए वह यह ब्रह्मोदन पकाने का यज्ञ कर रही है। इस यज्ञ के लिए अग्निमंथन करने वाले सप्तशीर्षण्य प्राणरूपी सप्तर्षि हैं २ जिनकी सहायता 'ब्रह्मणा संविदाना वाक् नामक प्रजा करती है। इसी प्रकार के यज्ञों से इन्द्र की वृद्धि और व्याप्ति होती है और इन्द्र को वृत्र-वध के लिए सामने लाया जा सकता है।४
यह महान् इन्द्र है जिससे साधक को अहंकार-रूप वृत्र-वध के लिए अपेक्षित ओज प्राप्त हो सकता है ।५ वह वज्री इतना महान् है कि रोदसी नामक द्यावापृथिवी अथवा अनेक अन्तरिक्ष (अंतरिक्षाणि) इसका विवेचन नहीं कर सकते, अपितु उसके बल और ओज से ही सब कुछ
-----
१.अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा ।
सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ।। -अथ ११.१.१
अदितिः पुत्रकामा ब्रह्मौदनमपचत्....तस्यै धाता चार्यमा च...मित्रश्च वरुणश्च...इन्द्रश्च विवस्वांश्चाजायेताम्, -तैब्रा.१.१.९.-१-२
२.प्राणा वै सप्त ऋषयः, मैसं.१.५.११
ये सप्तशीर्षण्याः पाणा आसन् ते सप्तर्षयोऽभवन् । -काठक संक ८६.२
३.अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपं ।।
तस्याऽसत् ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना।। - बृउ २.२३.४
४.यज्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपातमम्। होत्राभिरिन्द्रं वावृधुर्व्यानशुः।
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः ।।-ऋ.८ १२.२०-२१
५.ऋ.८.१२.२२-२३
देदीप्यमान हो जाता है ।१ अन्तरिक्ष के समान द्यौ और भूमि के भी अनेक रूप माने गए हैं, पर वे सब भी वज्री इन्द्र का विवेचन करने में असमर्थ हैं -
न द्याव इन्द्रम् ओजसा न अन्तरिक्षाणि वज्रिणम् ।
न विव्यचन्त भूमयः ।। ऋ.८.६.१५
वास्तव में यह महान् वज्री इन्द्र परब्रह्म परमात्मा है जो अनेकता में बिखरे हुए मनुष्य- व्यक्तित्व के लिए सर्वथा अगम्य है। इसी बात को बतलाने के लिए अनेक अन्तरिक्षों आदि को उसका विवेचन करने में असमर्थ बताया गया है । इस बिखरे हुए व्यक्तित्व का स्वामी वह जीव है जिसको एक मन्त्र में असुर सुपर्ण कहा गया है जब कि परब्रह्मरूप इन्द्र को सूर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है -
वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्गभीरवेपा असुरः सुनीथः ।
क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान।। ऋ.१.३५.७
इस मन्त्र के अनुसार, सुपर्ण (जीवात्मा ) अन्तरिक्षों को गंभीर कम्पन के साथ देख रहा है, परन्तु ब्रह्मरूप सूर्य का पता ही नहीं है । इस रहस्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, एक बार त्रिलोकी पर दृष्टि डालें ।
लोकत्रयी में अन्तरिक्ष
लोक में प्रचलित अवधारणा के अनुसार सबसे नीचे पृथिवी है और ऊपर द्युलोक है तथा इन दोनों के बीच अन्तरिक्ष स्थित है।
-----
१.न यं विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणम् ।
अमादिदस्य तित्विषे समोजसः ।। ऋ.८.१२.२४
कई स्थानों पर वेद मन्त्रों में भी इसी कल्पना को स्वीकार किया गया। उदाहरण के लिए अथर्ववेद के ४.१४.३ में साधक अपने आरोहणक्रम की चर्चा करता हुआ सर्वप्रथम पृथिवी का उल्लेख करता है, तत्पश्चात् अन्तरिक्ष और द्यौ का नाम लेकर पुनः वह द्यौ नाक की पीठ से "स्वः” नामक ज्योति तक पहुंचने की बात करता है-
पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम्।
दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ।।
अगले मन्त्र में कहा गया है कि इस ‘स्वः ज्योति’ को जाने वाले द्यौ पर आरोहण करते हैं, पर रोदसी की अपेक्षा नहीं करते, अपितु वे "विश्वतोधार यज्ञ” का विशेष रूप से विस्तार करते हैं -
स्व१र्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ।। अथ.४.१४.४
यहां रोदसी की अपेक्षा न करना और द्यौ की ओर आरोहण करते हुए "विश्वतोधार यज्ञ” का विस्तार करना साभिप्राय प्रतीत होता है। जैसा कि पूर्व अध्याय में उल्लिखित है, आद्योदात्त रोदसी प्राणापान-रूप द्यावापृथिवी का वह रूप है जिसे मनुष्य - व्यक्तित्व का पशु-स्तर माना जाता है और जो शरीर-केन्द्रित अहंकार-रूप वृत्र के कारण अनृत और दुरित का भण्डार बनकर मन-रूप प्रजापति को रुलाता है। इसीलिए उसका नाम रोदसी है। अतः इसकी अपेक्षा न करके ही यज्ञ का विस्तार हो सकता है, क्योंकि यह यज्ञ “विश्वतोधार” अर्थात् आन्तरिक विश्व को धारण करने वाला यज्ञ है। इसीलिए इस यज्ञ का विस्तार करने वाले "सु” के जानकार (सुविद्वांसः) कहे गए हैं । यह यज्ञ वस्तुतः वह अध्वर१ है जिसे प्राण-
----
१.यज्ञो वा अध्वरः, काठ ३१.११ ; तैआ ५.२.६०
साधना१ भी कहा जा सकता है । यह आन्तरिक यज्ञ वह श्रम, तप अथवा व्रतचर्या है जिसके द्वारा ऋषिगण उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं जिसे अथर्ववेद में मनुष्य के भीतर हिरण्यय कोश में स्थित बताया गया है । इस व्रतचर्या-रूप यज्ञ का सम्पादन उस ज्ञानाग्नि द्वारा ही सम्भव है जिसको मानुषी-त्रिलोकी और दैवी-त्रिलोकी की शक्तियों का चक्षु तथा सब देवताओं में प्रथम माना गया है और इस यज्ञ को करने वाले यजमान ही स्वः नामक ज्योतिर्मयी स्वस्ति अथवा स्वर्ग को प्राप्त करने के अधिकारी माने गए हैं -
अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषाणाम् ।
इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति।।-अथ.४.१४.५
इस स्वः नामक स्वस्ति या ज्योति की ओर आरोहण करने वाले लोग जिस "नाकं उत्तमं' को प्राप्त करने वाले कहे गए हैं वही वह द्यौ हो सकता है जिसको प्राप्त करने के लिए रोदसी की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं मानी गई, क्योंकि यह "सुकृतस्य लोक” है जबकि रोदसी अनृत और दुरित से युक्त होने के कारण रुलाने वाला माना गया है। यह बात अगले मन्त्र से सुस्पष्ट है -
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्। -अथ.१४.६.६ निस्संदेह, यह द्यौ उस द्यौ से भिन्न है जो रोदसी नामक द्यावापृथिवी के अन्तर्गत माना जा सकता है । "नाकं उत्तमं” कहा जाने वाला यह
------
१.प्राणोऽध्वरः, माश ७.३.१.५
२.ऋषयो ह वै स्वर्गं लोकं जिग्युः श्रमेण तपसा व्रतचर्येण, जै.२,२१७
३.तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गः ज्योतिषावृतः। अथ.१०-२.३१
द्यौ वस्तुतः बृहत् द्यौ है१ जिसको देवगण उक्त "विश्वतोधार यज्ञ द्वारा प्राप्त होते हैं । यही 'बृहत् द्यौ’ वह ‘मधु द्यौ’ है जिसे सभी साधक अपना पिता बनाना चाहते हैं।३
दूसरे शब्दों में, पृथिवी लोक से उक्त बृहत् द्यौ अथवा - नाकं उत्तमं तक आरोहण वस्तुतः एक आध्यात्मिक प्राण-साधना है इसीलिए इस आरोहण के लक्ष्य का एक नाम 'ओदनं’४ भी रखा गया है जो उदान नामक एक प्राण से निष्पन्न है। इस प्राण-साधना की व्रतचर्या के सात स्तर प्रतीत होते हैं । इन सातों का उल्लेख अथर्ववेद के व्रात्यकाण्ड में मिलता है। वहां इसी दृष्टि से उक्त वृतचर्या करने वाले व्रात्य के सप्तप्राण, सप्तअपान और सप्तव्यान कहे गए हैं।५ इस प्रसंग में स्पष्ट कहा गया है कि व्रात्य इस साधना के लिए सभी अन्तर्देशों में विविध रूप से परमेष्ठी हो कर तथा ब्रह्म को अन्नाद मानकर चलता है।६ यह ब्रह्म नामक अन्नाद ही अथर्ववेद में "ब्रह्मोदनः देवयानः स्वर्गः” कहा गया है और उसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है।७
----
१.माश ९.५.२.३; ९.१.२.३७
२.तैआ १०.६२.१
३.तैसं.४.२.९.३; मैसं.२.७.१६; माश १.७.२.१७
४.पंचौदनं पंचभिरङ्गुलिभिर्दर्व्योद्धर पंचधैतमोदनम् ।। प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम्।। अथ.४.१४.७
५.तस्य व्रात्यस्य सप्तप्राणाः,सप्तअपानाः,सप्तव्यानाः। - अथ.१५.२.८.१-२
६.स यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत् परमेष्ठी भूत्वानु व्यचलद् ब्रह्मान्नादं
कृत्वा । अथ.१५.१५.२३
७.अथ ११.१.२०
ओदन अथवा ब्रह्मौदन को लक्ष्य मानकर चलने वाली प्राण-साधना के जो सात स्तर हैं उनमें से प्रत्येक पर प्राण और अपान सक्रिय होकर व्यान नामक संधि को जन्म देते हैं । सातों स्तरों पर इन तीनों प्राणों का जो अलग अलग वर्णन किया गया है वह बहुत ही विचित्र है। प्रत्येक प्राण का सप्तविध स्वरूप निम्नलिखित है -
सप्तप्राणाः
१.तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ।
२.तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः।
३.तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणोभ्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः।
४.तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभुर्नामायं स पवमानः ।
५.तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य पंचमः प्राणो यो निर्नाम ता इमा आपः।
६.तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः ।
७.तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः।
-अथ.१५.१५.१-७
२ सप्त अपानाः
१ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी।
२ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका।
३ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य तृतीयोऽपानः सामावास्या।
४ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा।
५ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य पंचमोऽपानः सा दीक्षा।
६ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः ।
७ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः ।- अथ.१५.१६.१-७
३ सप्तव्यानाः
१ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः ।
२ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम्।
३ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य तृतीयो व्यानः सा द्यौः ।
४ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि।
५ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य पंचमो व्यानस्त ऋतवः ।
६ तस्य व्रात्यस्य। योऽस्य षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः।
७ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः। - अथ.१५.१७.१-७ यद्यपि तीनों प्राणों में से प्रत्येक के सप्त स्तरों का जो वर्णन अथर्ववेद से यहां प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ बातें अस्पष्ट होते हुए भी इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि व्यान के सात स्तरों में जो प्रथम तीन स्तर थे उनको क्रमशः भूमि,अन्तरिक्ष और द्यौ माना गया है । इसका अर्थ है कि यहां भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के व्यान के प्रतीक रूप में माना गया है। इस प्रसंग में जिसको “विश्वतोधार यज्ञ" कहा गया है प्राण उसका प्रातःस्तवन, अपान माध्यन्दिन-सवन और व्यान उपांशुसवन माना गया है। इसका अभिप्राय है कि "विश्वतोधार यज्ञ" का प्रतीक ही सोमयाग है जिसमें होने वाले प्रातः सवन, माध्यन्दिन-सवन और सायं-सवन सुविख्यात हैं। व्यान प्राण के प्रथम तीन स्तरों पर आश्रित पृथिवी,अन्तरिक्ष और द्यौ के त्रितय को क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश का समावेश करने वाली मानुषी-त्रिलोकी कहा जा सकता है।
-----
१.मैसं ४.८.७; ४.५.६; मा श.४.१.१.१
मनुष्य- व्यक्तित्व की यह त्रिलोकी व्यानप्राण के जिन प्रथम तीन स्तरों पर आश्रित है उनसे ऊपर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ के आधार पर दैवी-त्रिलोकी की अवधारणा हुई है। इसके अन्तर्गत मनोमय कोश का उर्ध्वगामी रूप विज्ञानमय और हिरण्ययकोश के साथ एकजुट हो जाता है। इसके बाद व्यान का जो सप्तम स्तर है उसको यहां संवत्सर नाम दिया गया है। संवत्सर का शाब्दिक अर्थ वत्स के साथ रहने वाला होता है। अतः इस स्तर की तुलना उस ज्योतिर्मण्डित स्वर्ग से कर सकते हैं जिस में आत्मा से युक्त ब्रह्म को विराजमान बताया गया है।१ यहां आत्मा वत्स है और ब्रह्म पिता है। वत्स से युक्त होने के कारण ब्रह्म को हो संवत्सर माना जा सकता है। इसी कारण संवत्सर को ब्रह्मवर्चस् का प्रदाता माना गया है। “संवत्सरो वै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदाता (तैसं २.I.२.६; ४.२) । संवत्सर का यह स्वर्ग ही वह "स्वः” नामक ज्योति है जिसे न केवल उक्त प्राण-साधना का लक्ष्य माना गया है अपितु स्वर्ग भी कहा गया है।२ इसी को प्राप्त करके साधक अमृत हो सकता है३ क्योंकि यह “स्वः” अथवा स्वर्ग लोक ही अमृतत्व कहा गया है ।४
सप्तलोकों की परिकल्पना
इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी आन्तरिक प्राण-साधना के अन्तर्गत व्यान के इन सात स्तरों को ही सप्तलोक माना गया है। जैमिनीय
----------------------
१.तस्मिन् यद् यक्षं आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः । अथ.१०.२.३२
२.स्वगों लोकः स्वः, जैब्रा.३.६९
३.यदा वै स्वर्गच्छति अथ अमृतो भवति, जैब्रा १.१३२
४.मैसं १.१०.१ ७ काठक सं.३६.११
ब्राह्मण इन लोकों में से प्रथम तीन को क्रमशः उपोदक, ऋतधाम और अपराजित नाम देता है और इसके पश्चात् चतुर्थ, पंचम और षष्ठ लोक को क्रमशः अधिदिवः, प्रदिवः और रोचनः नाम देता है। सप्तम को विष्टप् कहकर उसी को ब्रह्मलोक कहता है और उसमें सत्य को प्रकाशित होता हुआ मानता है -- स यद् भूर्भुव स्वरिति व्याहरत् त एवेमे त्रयो लोका अभवन्न् उपोदक ऋतधामाऽपराजितः । अथ करज् जनद् वृधद् इति व्याहरत् त एवेतेऽपरे लोका अभवन्न् अधिदिवः प्रदिवो रोचनः। विष्टप् एव सप्तमो ब्रह्मलोको यस्मिन् एतत् सत्यं भाति । तमेषा देवता सत्यं भूत्वानुप्राविशत्। जै ३.३८४ (तु.जै ३.८०)। इन सप्तलोकों की तुलना उन सप्त व्याहृतियों से की जाती है जिन्हें क्रमशः भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यं कहा जाता है। इन व्याहृतियों में से भूः, भुवः, स्वः और सत्यम् का तो स्पष्ट उल्लेख यहां किया ही गया है, जबकि पंचमी जनत् व्याहृति में जनः को देखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में चतुर्थ व्याहृति करत् को "महः " के स्थान पर और "वृधत्" को 'तपः के स्थान पर माना जा सकता है, परन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इस सप्तमलोक को यहां विष्टप्, ब्रह्मलोक और सत्यम् कहा गया है। वह वस्तुतः स्वः, स्वर्ग, ओदन अथवा ब्रह्मौदन नाम से उक्त प्राण-साधना अथवा आन्तरिक "विश्वतोधार यज्ञ” का लक्ष्य माना गया है। इसलिए यहां जो "स्वः” नाम की तीसरी व्याहृति है उस को इस सप्तम रूप से भिन्न मानना पड़ेगा। सभी व्याहृतियों का अभिप्राय केवल अभिव्यक्तियों से है । अतः उक्त उद्धरण में जब तृतीयलोक का निर्माण स्वः नामक व्याहृति के साथ कहा जाता है तो इसका तात्पर्य यही होता है कि इस स्तर पर सप्तमलोक के स्वः या स्वर्ग की किंचित् झलक या स्मृति प्रारम्भ हो जाती है ।
इसी दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेद १०.१२४.६ में सोम को आमन्त्रित करता हुआ इन्द्र “इदं स्वः इदमिदास वामं, अयं प्रकाश ऊर्ध्वन्तरिक्षम् ' को याद करके वृत्र-वध का प्रस्ताव करता है। वृत्र-वध के फलस्वरूप ही वरुण "आपः " की सृष्टि करता है।१ इस क्रिया की ओर ही उक्त करत् नामक व्याहृति का संकेत है, जबकि "क्षेमं कृण्वाना जनयो न सिन्धवः' कहकर “जनत" नामक व्याहृति की ओर इंगित किया गया है।२ व्यान के छठे स्तर पर जिस वृधद् का उल्लेख किया गया है उसकी झलक "ता अस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं सचन्ते”३ में देखी जा सकती है, क्योंकि ज्येष्ठ इन्द्रिय का सेवन करने वाले आपः निस्संदेह वर्धनशील कहे जा सकते हैं। वे ही अन्ततोगत्वा व्यान के सप्तम स्तर पर इन्द्र-ब्रह्म के उस सत्य रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं जिसे दिव्य आपः का "सयुजं हंसम्" कहा गया है -
बीभत्सूनां सयुजं हंस माहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्।
अनुष्टुभमनु चर्चूर्यमाणमिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनीषा।। - ऋ.१०.१२४.१
आपः नामक अन्तरिक्ष
इस प्रकार ऋ.१०.१२४ में, जिस स्वः, वामम्, प्रकाश और उरु अन्तरिक्ष का नाम लेकर वृत्र-वध का प्रस्ताव किया गया था, उसकी परिणति न केवल उरु अन्तरिक्ष नामक प्रकाश-समुद्र में होती है, अपितु
-----
१.वरुणो निरपः सृजत्, - ऋ.१०.१२४.७
२.वही
३.वही, १०.१२४.८
सिंधवः अथवा आपः की सृष्टि के साथ-साथ उन सबके “सयुजं हंसम्" (इन्द्रं ब्रह्म) के साक्षात्कार में भी होती है। इस प्रकार हम निघण्टु के अन्तरिक्षनामों में 'आपः' के समावेश में औचित्य खोजने की आशा कर सकते हैं । प्रकाशात्मक "उरु अन्तरिक्ष वस्तुतः स्वर्ग अथवा ब्रह्माण्डीय प्रकाश-सिन्धु है। अतः उसके साथ आपः का समीकरण तब तक उचित नहीं कह सकते जब तक हम आपः को सामान्य भौतिक जल का वाचक मानेंगे, परन्तु, जैसा कि उपर्युक्त मन्त्र मंक कहा गया है, ये "दिव्य आपः“ हैं जिनका "सयुज हंस” इन्द्र है। "सयुज हंस" कहने का अभिप्राय यह है कि इन्द्र इन दिव्य आपः से सर्वथा अभिन्न है। वास्तव में आपः ब्रह्म की शक्ति है जो निस्संदेह अपने शक्तिमान से अविनाभाव सम्बन्ध रखती है। कालिदास ने अपने विश्व-प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् के मंगलाचरण में सर्वप्रथम स्रष्टा की आद्यासृष्टि को याद किया जिसे टीकाकार राघव ने आपः बताया है और अपने मत की पुष्टि में मनुस्मृति का वाक्य 'अप एव ससर्जादौ (१,८) उद्धृत किया है। जैसा कि हम देख चुके हैं, यह आद्यासृष्टि दिव्य आपः की सृष्टि है जो प्राण-साधना के अन्तर्गत सात व्यान-स्तरों में से अंतिम स्तर में प्रकट होती है। इसलिए यह कहना कदापि अनुचित न होगा कि आपः की आद्यासृष्टि से अभिप्राय दिव्य-प्राणों की आद्यासृष्टि से है।
अतएव अथर्ववेद के प्राण-सूक्त में प्राण के वर्णन में जलवृष्टि के रूपक का उपयोग करते हुए प्राण को क्रन्दन अथवा गर्जन करने वाला तथा चमकने एवं बरसने वाला बताया गया है।१ प्राणों का भेषज जहां
-----
१.नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे ।
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ।। अथ.११.६.२
स्पृहणीय१ है, वहीं आपः को "भिषजः मातृतमाः२तथा सम्पूर्ण विश्व की जनित्री कहा गया है। आपः मनुष्य के भीतर ऐसी भेषज भर देते हैं कि वह सूर्य को सदा देखने में समर्थ होता है।३ प्राण प्रजापति हैं और आपः भी प्रजापति की तरह प्रजा उत्पन्न करने में समर्थ हैं४ और आपः को प्रजापति परमेष्ठी भी कहा जाता है।५ अतः कोई आश्चर्य नहीं कि "आपो वै प्राणाः की उक्ति वैदिक वाङ्मय में बहुत लोकप्रिय हुई है।६ आपः ही आदि में प्रजापति-रूप में उत्पन्न हुए जिनके मन में यह इच्छा हुई कि हम सृष्टि करें ।७
आदि सृष्टि होने के कारण ही ऋग्वेद में “आपो देवीः प्रथमजाः” उक्ति मिलती है और गोपथ ब्राह्मण में ऋग्वेदादि संहिताओं में आपः से होने वाली सृष्टि की व्याख्या विभिन्न अर्थवादी आख्यानों ओर अर्थान्वाख्यानों द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए यहां गोपथ-ब्राह्मण के सृष्टि-वर्णन को ‘भावी वेदभाष्य के संदर्भ-सूत्र’ से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।
गोपथब्राह्मण का सृष्टिवर्णन
मानव के देशकालातीत स्तर पर एकमात्र ब्रह्म है। वह अपने
-----
१.या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी।।
अथो यद् भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे।। अथ ११.६.९
२.ऋ.६.५०.७
३.वही.१०.९.७
४.माश ११.१.६.१
५.आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति।
माश ८.२.३.१३
६.काश ४.८.२.२; मा श ३.८.२.४; जैउ ३ः१०.९; तैआ १.२६.५
७.आपो वा इदमासन्सलिलमेव। स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्।
तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत। इदं सृजेयमिति, तैआ १.२३.१
को “महद् यक्षम्” रूप में देखता है, तो एक वैसा ही दूसरा निर्माण करने की इच्छा से तप करता है। इस द्वितीय महद् यक्षं का नाम "सुवेद” (सुन्दरं वेदनं ) है क्योंकि यह आनन्दकर अनुभूति देता है । इसका उद्भव ऐसा सहज और सुखद है जैसे ललाट पर स्वेद। अतः सुवेद को "स्वेद" कहा गया। यही स्वेद बाद में सब रोमकूपों से धाराओं के रूप में फूट पड़ा । स्वेद एक से अनेक हो गया। सुवेद उस सबका बीज है ।
अनेकरूपा धारा वस्तुतः व्यष्टिगत पुरुष की प्रकृति अथवा आह्लादिनी शक्ति है। धारक होने से धाराः, जनक होने से जायाः और आपक अथवा व्यापक होने से उसी का नाम आपः है। इस मूल प्रकृति के इन त्रिविध रूपों की तुलना सांख्य की प्रकृति के क्रमशः सत्व, रजस् तथा तमस् से की जा सकती है। वैदिक साहित्य में इसी प्रथम सृष्टि को प्रायः आपः की आद्या१ सृष्टि माना जाता है । सुवेद आनन्दमय कोश का वेद है जो उद्धरणीय ब्रह्म-वीर्य भी है।२
ये आपः शान्त और अशान्त भेद से दो रूप ग्रहण करते हैं। शान्ताः आपः में पड़ा हुआ ब्रह्म-वीर्य भृगु-प्राण बनता है, तो अशान्ताः आपः में पड़ा रेतस् समुद्र को आवृत कर लेता है। शान्ताः और अशान्ताः आपः की तुलना अघमर्षण- सूक्त (ऋ.१०.१९०) की क्रमशः रात्री और समुद्रो अर्णवः से कर सकते हैं। भृगु ही वह वत्स है जिससे युक्त हो कर विज्ञानमय पुरुष “संवत्सर" कहलाता है। (वही, २)
----
१.देखिए, डॉo फतहसिंह- कृत "मानवता को वेदों को देन" प्रथम
अध्याय ।
२.यस्मात् कोशाद् उद् अभराम वेदं, तस्मिन्न् अन्तर् अव दध्म एनम्।
कृतम् इष्टं ब्रह्मणो वीर्येण, तेन मा देवाः तपसावतेह । अ १९.७२.१
विज्ञानमय का एक ऊर्ध्वमुखी शान्त पक्ष है, तो दूसरा अर्वाक् गति करने वाला तथा तन की ओर उन्मुख पक्ष । पहले की दृष्टि से सुवेद "ब्रह्मवेद “ कहलाता है तो दूसरे की दृष्टि से 'अथर्ववेद’ । प्रस्तुत गोपथीय सृष्टिवर्णन में, प्रथम (शान्त) पक्ष के संदर्भ से विज्ञानमय पुरुष को भृगु कहा गया । ऋग्वेद में इसी को चेतन, भृगवाण अग्नि (४.७.२; ४) कहा जाता है। गोपथ१ में भृगु के वायु, मातरिश्वा, पवमान और वात नाम से, चार पक्ष माने गए हैं। पर, इस शान्त पक्ष की सृष्टि में अहम् की अनुभूति नहीं होती - न न्व् अविदम् अहम् इति (गो १ • ४) अतः यह विज्ञानमय का अहंपूर्व पक्ष है, जबकि अथर्ववेद वाले, अर्वाक् गति से युक्त, विज्ञानमय को अहं-पक्ष कहा जा सकता है। यही अथर्वा प्रजापति है जो मनोमय की नानारूपात्मक सृष्टि करने में सक्षम है (गो १.४)।
मनोमय-सृष्टि से पूर्व, बीस आथर्वण ऋषियों और बीस आथर्वण आर्षेयों के मन्त्रों के रूप में आथर्वण वेद, "ऊर्ध्व अक्षरं मनः” ( Super mind) की सृष्टि का उल्लेख है। इसी को ओम् नामक महाव्याहृति भी कहा (गो १.५८) गया है। यह विज्ञानमय पुरुष का अहंपूर्व पक्ष है जो मनोमयादि की सृष्टि के लिए तैयार है। यही अथर्वा हो कर मनोमय सृष्टि करता है ।
• विज्ञानमय कोश के इन दोनों पक्षों को सूचित करने के लिए ही, दो विपरीत त्रिभुजों वाले श्री-यंत्र का प्रयोग होता है जिस में उर्ध्वमुखी त्रिभुज अहंपूर्व का द्योतक है और अधोमुखी त्रिभुज अहंपक्ष का -
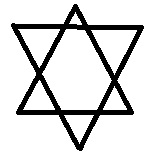
------
१.गो १.४
अघमर्षण-सूक्त में प्रथम पक्ष को सत्यं की, तो द्वितीय पक्ष को ऋतम् की प्रवृत्ति कहा गया है। इन दोनों पक्षों के आधार पर ही वेद में द्विमूर्धा आर्त्व्य की, तो रोम देश में द्विमुख जनुस देवता की कल्पना हुई है। आनन्दमय (हिरण्यय) कोश में, ये दोनों अभिन्नरूपेण संपृक्त होते हैं जिसकी सूचक एक त्रिभुजाकार दीपशिखा है। विज्ञानमय में, एक पक्ष चिर शांति के लिए, तो दूसरा सतत् अशांति (परिवर्तन) के लिए उद्यत है, जबकि मनोमय स्तर पर दोनों पक्ष एक-दूसरे से होड़ करते हुए से आंखमिचौनी का खेल शुरू कर देते हैं । इसी का प्रतीक अघमर्षणसूक्त (ऋ..१०.१९०.२) में "अहोरात्राणि” है। विज्ञानमय में,उर्ध्वमुखी त्रिभुज रात्रि, चन्द्रमा और शान्त आपः का प्रतीक है, तो अधोमुखी त्रिभुज अहन् (दिन) सूर्य और अशान्त आपः का सूचक है। अहंपूर्व सत्यं और अहंपक्षीय ऋतम् दोनों विज्ञानमय में, समन्वित साम्यावस्था में, होते हैं ।
मनोमय स्तर पर बात तब बदल जाती है जब स्रष्टा नानारूपात्मक सृष्टि को ही अहम् समझने लगता है। इसी भावना का नाम अहंकार है। इसके फलस्वरूप, अज्ञानांधकार की महानिशा छा जाती है। यही "दीर्घं तमः” वृत्र है ( ऋ.१.३२.१०), जिसको नष्ट करने वाली दृष्टि अघमर्षण दृष्टि है। वृत्र-वध होते ही पूर्वोक्त सूर्याचन्द्रमसौ यधापूर्व हो जाते हैं और वृत्र-रूप दीर्घंतमः के कारण मनोमय,प्राणमय एवं अन्नमय कोश-रूप क्रमशः द्यौ,अन्तरिक्ष और पृथिवी की जो "दिव्य स्वः “ नामक ज्योति नष्ट हो चुकी थी वह त्रिलोकी पुनः अस्तित्व में आ जाती है -
सूर्याचन्द्रमसौ धाता, यथापूर्वम् अकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम् अथो स्वः ।। ऋ.१०.१९०.३
इस दृष्टि के लिए, गोपथ के अनुसार, पूर्वोक्त अथर्वा प्रजापति ओम् नामक "उर्ध्वमनः अक्षरं” की महाव्याहृति उत्पन्न करता है और तत्पश्चात् उक्त तीनों लोकों के साथ-साथ अग्नि, वायु और आदित्य तथा उनसे सम्बन्धित ऋक्, यजुः और साम सहित भूः, भुवः एवं स्वः नामक महाव्याहृतियों को प्रादुर्भूत करता (गो• १.६) है ।
यह वांछित सृष्टि तभी सम्भव होती है जब अशान्त आपः - रूप समुद्र भगवान् को राजा वरण करते हैं । वरण के कारण उस का नाम वरुण होता है। वह (अशान्त) समुद्र से मुक्त होता है (अमुच्यत) । अतः उसका नाम मुच्यु है। वही मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु के अंगों से जो रस निकला वह अंगिरा कहा गया । अंगिरा से बीस आंगिरस ऋषि और बीस आंगिरस आर्षेय उपजे । इन सबके मन्त्रों से आंगिरस वेद बना। आंगिरस वेद से “जनत्" नामक महाव्याहृति पैदा हुई । तब अंगिरा ने प्राची, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा और उर्ध्वा दिशाओं को देखा । उनको सहायता से निम्नलिखित पंच वेदों और उनकी पंच महाव्याहृतियों को उत्पन्न किया –
पंच वेद पंच महाव्याहृतियां
१ सर्पवेद वर्धत्
२ पिशाचवेद करत्
३ असुरवेद रुहत्
४ इतिहासवेद महत्
५ पुराणवेद तत्
गोपथ(१.९.१०) के इस वर्णन में आगे, आवत् तथा परावत् (मनोमय के अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी) आपः से शम् नामक “ऊर्ध्व अक्षरं" तत्व के उद्भव का उल्लेख है। उसी से उक्त "तत्" नामक महाव्याहृति.उपजती है (वही, ११) । तत्पश्चात् वह अपने मन से चन्द्रमा, नखों से नक्षत्र, लोमों से ओषधि - वनस्पतियां तथा दक्ष प्राणों से अन्य अनेक देवों को पैदा करता है और फिर, त्रिवृत् सप्ततंतु एवं एकविंशतिसंस्थ यज्ञ को जन्म (वही, १२) देता है।
शम् सहित उक्त पंच व्याहृतियों के उत्पादन के पश्चात्, ब्रह्म पुष्कर में ब्रह्मा को पैदा करता है जो ओम् नामक एकाक्षर ऋक् को जन्म देता है (वही, १.१६-१७)। ओम् नामक वह एकाक्षर ऋक् ऋक् में ऋक्, यजु में यजु, साम में साम, सूत्र में सूत्र, ब्राह्मण में ब्राह्मण, श्लोक में श्लोक और प्रणव में प्रणव है ( वही, २३)।
वेदों और व्याहृतियों का मनोविज्ञान
यह सारा सृष्टि-वर्णन वेदों और व्याहृतियों पर आधारित है। वेद और व्याहृतियां दो प्रकार की हैं जिनको दो प्रकार के आपः (शान्ताः और अशान्ताः) से सम्बद्ध बताया गया है। लोक में आपः का अर्थ जल अवश्य है पर वेद में वह प्राण-तत्त्व१ का नाम है। इसीलिए, ब्राह्मण ग्रान्ध बार-बार (तां ९.९.९.४; तै ३.२.५.२; जैउ ३.२.५.९) "प्राणा वा आपः “ की रट लगाते है और, आपः के समान, प्राणों२
-------
१.आपो वै प्राणाः,काश ४.८.२.२; माश ३.८.२.४; जैउ ३.१०९; तैआ १.२६.५ २.अ ११.४.I; मा श १४.८.१३.३; १४.२.२.३४
को भी इदं सर्वं को व्याप्त करने वाला (माश १.१.१.१४; २.१.१.४) कहा जाता है। अथर्ववेद में इसीलिए प्राणों के वर्णन में भी जल-वृष्टि के रूपक का प्रयोग हुआ है, यथा
यत् प्राण स्तनयित्नुनाभिक्रन्दत्य् ओषधीः।
प्र वीयन्ते गर्भान् दधतेथो बह्वीर वि जायन्ते।।
यत् प्राण ऋताव् आगतेभिक्रन्दत्य् ओषधीः ।
सर्वं तदा प्र मोदते यत् किं च भूम्याम् अधि ।।
यदा प्राणो अभ्य् अवर्षीद् वर्षेण पृथिवीं महीम्।
पशवस् तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ।।
अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन् । अ ११.४.३-६
अतः आपः को जब शान्ताः और अशान्ताः कहा जाता है तो इससे प्राणों को ही शान्त और अशान्त समझना चाहिए। आपः दिव्य प्राणों का ही भौतिक प्रतीक है। विज्ञानमय स्तर पर,ऊर्ध्वमुखी प्राण शान्त कहे जाते हैं, तो अधोमुखी प्राण, मनोमय की ओर जाने के लिए गतिशील होने से, अशांत कहे जाते हैं । मनोमय में पहुंचकर जब वे अहंकार-रूप वृत्र को वरण करते हैं तो वे घोर अशान्त हो जाते हैं । जब वे भगवान्१ को राजा वरण करते हैं तो सत्यानृत२ का विवेक रखने वाले वरुण का अभिषेक होता है। वरुण का विवेक उसे अशांत समुद्र से परे पहुंचाने में समर्थ है। वह अशांत समुद्र से मुक्त अवस्था है जो कि मनोमय की दृष्टि से मृत्यु भी कही जा सकती है क्योंकि वहां मनोमय की अनेकता और अशांति नहीं है। इसी को कभी-कभी मनोनाश वा "विनशन" कहा जाता है जहां जलप्लावनग्रस्त मनु की नाव हिमालय
१.तुः परा दस्यून् ददती देवपीयून् इन्द्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम्। -अ १२.१.३७
२.सत्यानृते अवपश्यञ् जनानाम् । ऋ.७.४९.३
से संपर्क करती है, अर्थात, अशांत व्यक्तित्व शांत स्तर को स्पर्श करता है।
पर यह परिवर्तन एक्दम नहीं हो जाता। वरुण शान्त आपः (प्राण) से संबंधित पूर्वोक्त भृगु अग्नि को वारुणि बनाता है और स्वयं अंगिरा बनकर मनोमय से लेकर अन्नमय तक सब अंगों के रसों (आंगिरस प्राणों) को अपना अंगभूत करके और स्वयं उनका अंगी बनकर उन्हें अपनी शक्ति देकर अपना अंगिराः (अंगी + राः) नाम सार्थक करता है। इसके परिणामस्वरूप ही जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के प्रतीक सर्पवेदादि वेद, एवं वर्धत, आदि व्याहृतियां हैं। अंगिरा "शम्" की ‘राति’ सभी स्तरों पर वितरित करता है जिससे प्रत्येक स्तर का वृत्र बदलकर वारुण (विवेकशील) वृत्त का हो जाता है क्योंकि जो वृत्तियां पहले अशांति का कारण थीं उनका अब सदुपयोग होने लगता है। इसीलिए उनको वेद कहा जाता है- विष उगलने वाला क्रोध - रूप सर्प अब शुभ की रक्षा के लिए अशुभद्वेषी बनकर ह्रास के स्थान पर वृद्धि का कारण बनता है; अतः सर्पवेद की "वर्धत्” व्याहृति है। रूप (पेश) लोभी काम-रूप पिशाच मांसल भोगों का लोलुप होने के बजाय सुन्दर कला-कृतियों के निमाण में बदल जाता है, अतः पिशाच-वेद की निर्माणपरक “करत्” व्या हृति है। महाप्राणता (असु) का लोभी स्वार्थवाद अब भौतिक बल और परपीडन के बदले आध्यात्मिक आरोहण के लिए प्रयुक्त होता है; अतः असुर-वेद की “रुहत्” व्याहृति है। पुरातनता (इतिहास) प्रेमी अंधा रूढ़िवाद अब विवेकशील इतिहास-प्रेम में बदलकर महत्त्व का पोषक होता है; अतः इतिहास-वेद की व्याहृति "महत्" कहलाती है। शरीर-रूप पुर के अन (प्राण) का प्रेमी भौतिकवाद अब शारीरिक प्राणबल को आध्यात्मिक सत्य (तत्) का लक्ष्य स्वीकार कर लेता है; अतएव वह पुराणवेद कहलाता है जिसकी व्याहृति का नाम “तत्” है। इस प्रकार, अशान्त आपः की "तत्" नामक व्याहृति को लाने में पूर्वोक्त "शम्” व्याहृति का पुट ही मूल कारण है।
इन पंच व्याहृतियों के रूप में शम् की उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणामस्वरूप हृदयकमल-रूप पुष्कर में ब्रह्म अपने ज्येष्ठपुत्र१ 'ओम्' व्याहृति को जन्म देता है। वही एकाक्षर ऋक् वा एकाक्षर मंत्र है। इसी को ज्येष्ठ प्राण२ भी कहा जाता है। यही ब्रह्मवेद का “आथर्वणशुक्र” है जिससे सब मंत्र प्रादुर्भूत होते हैं।३ यही वह ऋक् हे जो मानवव्यक्तित्त्व में स्थित यज्ञ के आगे पीछे, भीतर (विश्वतः) और बाहर (सर्वतः) सर्वत्र युक्त होकर उसे विस्तार देने का प्रयत्न करती है तथा जिसके अक्षर, परम व्योम में विश्वे देवाः समाहित होते कहे जाते हैं।४
विश्वे देवाः
ओम् नामक व्याहृति, मंत्र वा ऋक् के परम व्योम में समाहित होने वाले विश्वे देवाः भी तो वस्तुतः अनेक प्राण ही हैं। आपः प्राण हैं; अतः आपः५ को भी "वैश्वदेवीः६ कहा जाता है। ओम् नामक
----
१.त ओंकारं ब्रह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं ददृशुः, गो. १.२३
२.अ १०.८
३.सैषा एकाक्षरा ऋक् ब्रह्मणस् तपसोग्रे प्रादुर्बभूव ब्रह्मवेदस्याथर्वणे
शुक्रम्। अत एव मन्त्राः प्रादुर्बभूवुः, गो ।.२२.
४.अ १०.८.१०; ऋ.१.१६४.३९, इसकी व्याख्या के लिए देखिए, गो १.१४
५.प्राणा व विश्वे देवाः । तैसं ५.२.२.१; ४.६.१; मै १.५.११; काठ १९.१२; २१.८; क ३१.२; माश १४.२.२.३७
६.वैश्वदेवीर् आपः। मै ४.५.२
महाव्याहृति वा ऋक् में विश्वे देवाः के समाहित होने का अर्थ है सब प्राणों का समाहित होना । दूसरे शब्दों में, ओम् प्राणों (आपः) की केन्द्रीभूत वा एकीभूत स्थिति का वाचक है।
इस स्थिति का वाचक विश् शब्द भी है। अतः विश् को विश्वे देवाः बताने का भी यही अर्थ है कि वे विश् में समाहित माने जाते हैं । विश् से , वस्तुतः,पांच देवगण१ प्रादुर्भूत माने गए हैं – १.वसवः २.रुद्राः ३.आदित्याः ४.विश्वेदेवाः और ५.मरुतः। इन पांचों में से, विश्वे देवाः के समान, मरुतः 'स्वापयः ' प्राण हैं, प्राणों द्वारा अवकीर्ण हैं और प्राणों के साथ कमों में प्रवेश करते हैं ।२ इसी तरह आदित्यों को भी प्राण कहा जाता है, क्योंकि वे सर्व का आदान करते हैं।३ आत्मा और दश प्राणों को मिलाकर ११ रुद्र कहे गए हैं।४ प्राणों को वसवः भी कहते हैं क्योंकि, वे ही सर्व वसु का आदान करते हैं।५
इसलिए, कम से कम ये पंच देवगण तो निस्संदेह प्राण ही हैं। वैसे, किन्हीं द्रविणोदाः देवाः (मै ३.२.१), अपाव्याः देवाः। तै ३.८.१७.५; माश ६.७.२.३; ६.३.१.१५).धिष्ण्याः देवाः (माश ७.१.१.२४), मनुजाताः देवाः (काठ २३.५).मनोजाता मनोयुजः देवाः(तैसं ६.१.४.५; काठ २३.५), मरीचिपाः देवाः (काठ २७.१; क ४२.१०) तथा वयोनाधाः देवाः (माश ८.२.२.८) को भी यत्र तत्र
-----
१.स विशम् असृजत यान्य् एतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो
रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। माश १४.४.२.२४
२.प्राणो वे मरुतः स्वापयः। ऐ ३.१६; मरुतः प्राणेन (अवकीर्णः प्रविशति)
जै १.३६२ मरुतः प्राणैः। तैआ २.१८.१
३.प्राणा वा आदित्याः । प्राणा हीदं सर्वम् आददते। जैउ ४.२.१.९
४.दश पुरुषे प्राणाः। आत्मैकादशः। ते यदोक्रामन्तो यन्त अध
रोदयन्ति। तस्माद् रुद्राः। जै २.७७
५.प्राणा वै वसवः। प्राणाः हीदं सर्वं वसु आददते। -तै ३.२.३.३; ५.२; जैउ ४.२.१.३
प्राणाः ही बताया गया है। साध्याः (माश १०.२.२.३) और स्वभवसः (तैसं ६.४.५.४) देव भी प्राण हैं।
कुछ देवमिथुन वा देवद्वन्द्व कहे जाने वाले देवों को “प्राणापानौ” कहा जाता है, यथा, प्राणापानौ, मित्रावरुणौ (तां ६.१०.५; ९.८.१६; ३.३.६.९).प्राणापानौ वै मित्रावरुणौ (काठ २९.१; ३०.३; क ४५.१; जै १.३४७)। अश्विनौ भी "पाणापानौ' हैं क्योंकि मित्रावरुणौ जिसके अपरपाद हैं अश्विनौ उसी के दो पूर्वपाद (तैआ २.१९.२) हैं। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार, द्यावापृथिवी, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ, अश्विनौ ही नहीं, वैदिक साहित्य में जो भी द्वन्द्व वा दिव्यमिथुन कहा जाता है वह पराक् और पूर्वाक् भेद से स्तोमद्वन्द्व माना गया है - ताव् एवैतो स्तोमौ अभवताम् च। तौ प्राणापानौ, ते अहोरात्रे, तौ पूर्वपक्षापरपक्षौ, ताव् इमौ लोकौ (द्यावापृथिवी), ताव् इन्द्राग्नी, तौ मित्रावरुणौ, ताव अश्विनौ, तद् दैव्यं मिथुनं यद् इदं किं च द्वन्द्वं तद् अभवताम् (जै ३.३३४)। इनको "स्तोमद्वन्द्व” कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि सब स्तोम वस्तुतः प्राण ही हैं - प्राणाः वै स्तोमाः (जै २.१३३), प्राणाः वै स्तोमाः सुरभयः ( तै ३.९.७.५; माश ८.४.१.३)|
प्राण को अलग-अलग वायु (माश ५.२.४.१०) वैश्वानर (मै ४.६.६), बृहस्पति (माश १४.४.I.२२ ), ब्रह्मणस्पति(माश ।४.४.१.२३), सोम(कौ ९.६; माश ४.४.१.५), वरुण(गो २.४.११) और वात(माश ५.२.४.९) बताया गया है। धर्मधृत देव कहे जाने वाले सोम, इन्द्र, वरुण, मित्र अग्नि भी प्राण हैं।१ आदित्यगण से भिन्न एक
-----------
१.सोम इन्द्रो वरणो मित्रो अग्निस् ते देवा धर्मधृतो धर्म । धारयन्ति एते वे देवा धर्मधृतो यद् इमे प्राणाः ।। -मै ४.४.२
आदित्य (एकवचन) भी प्राण (जैउ ३.१.४.९; ४.११.१.११) हैं और स्वयं ब्रह्म (जैउ ३.१.४.९) को भी प्राण कहा गया।
निष्कर्ष
इस सृष्टि के वर्णन के आलोक में एक प्राण रूपी देव से अनेक प्राण-देवों की सृष्टि वस्तुतः शक्तिमान ब्रह्म की वाक् नामक शक्ति से होने वाली अनेकतामयी सृष्टि को सरलता से समझा जा सकता है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार प्राणों में वाक् सप्तमी है।१ ऐतरेयब्राह्मण की वाक् सप्तविध बोलती है। तैत्तिरीय संहिता वाक् को सब प्राणों में उत्तम एक ज्योति मानती है।३ प्राण को ही वाक् कहा गया है।४ जिस प्रकार ऊपर प्राण को ब्रह्म कहा गया है, उसी प्रकार वाक् को भी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वाक् ब्रह्म की शक्ति है जिसके द्वारा वह सृष्टि करता है६ और ब्रह्म को वाक् का परमव्योम भी कहा जाता है।७
इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जिस प्रकार पहले प्राण, अपान और व्यान के सात स्तरों में से पहला स्तर अन्य छह स्तरों में विभक्त होता है उसी प्रकार जो वाक् सप्तधा बोलने वाली कही गई है उसी
------
१.इयं वाक् सप्तमी प्राणानाम्, मैसं ३.१.९
२.सप्तधा वै वागवदत्, ऐब्रा २.१७
३.तैसं ५.१.९.१; ५.३.२.३; ६.६.११.६; काठक सं.१९.१०;
कपि सं ३०.८.
४.मैसं ३.२.८; माश १.१.२.१४, तैआ ३.४.१
५.जैब्रा १.८२; २७२; २.७८; ३.३०७; वा क् वै ब्रह्म, ऐब्रा ६.३; जैब्रा
।.१०, २.११५; १४०; १७८ माश २.१.४.१०; १४.४.१; २३; ६.१०.५आदि।
६.काठक सं० ४३.४
७.ब्रह्मैव वाचः परमं व्योम, तैसं ७.४.१८.२; काठक ४४.७;
तैब्रा ३.९.५.५
को “षड् अहानि" में विभक्त होता हुआ बताया गया है और उससे परे उसका एक अतिवक्ता रूप भी माना गया है।१ आश्चर्य की बात यह है जहां प्राण२ को अन्तरिक्ष कहा गया वहीं वाक्३ को भी अन्तरिक्ष कहा गया है। अतः अन्तरिक्ष का भी जो प्रथम रूप है उसी को छह अन्य अन्तरिक्षों में विभक्त माना जा सकता है। प्रथम "उरु अन्तरिक्ष है जो व्यष्टिगत और समष्टिगत जगत् में समान रूप से छह अन्तरिक्षों में विभक्त हुआ प्रतीत होता है ।
इसलिए अन्तरिक्ष को व्यष्टिगत पुरुष की वह आन्तरिक शक्ति कह सकते हैं जो 'अपां धारा संतता" कहलाने वाली ऊर्ध्वा वाक् है।४ इसी तरह जब प्राण से प्रजापति लोकों की सृष्टि करता हुआ कहा जाता है५ तो वाक् के समान प्राण को भी समस्त सृष्टि का स्रोत माना गया प्रतीत होता है। इसीलिए पूर्वोक्त विवेचन में प्राण, अपान और व्यान की दृष्टि से सप्तलोकों के त्रिविध वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। जब अन्तरिक्ष को प्राण कहा जाता है तो वह भी अनेकविध सृष्टि का स्रोत होने से सम्पूर्ण प्रजाओं को आत्मसात् करने की दृष्टि से 'अन्तरिक्षमिमाः प्रजाः' की उक्ति ग्रहण करता है।६ जब आत्मा को अन्तरिक्षम्' कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यही है कि अन्तरिक्ष आत्मा की शक्ति है जो स्वयं आत्मा-रूप ही है।७
------
१.मैसं ३.७.६
२.तैसं ५.६.८.५; जैब्रा १.३०७ मा श.७.५.१.२६
३.वागिति अन्तरिक्षम्, जैउ ४.११.१.११
४.सा (वाक्) ऊर्ध्वा उदातनोत् यथा अपां धारा संतता एवम्। -तांब्रा २०.१४.२ ५.कौ ब्रा ६.१० तुः काठ सं १७.७
६.मैसं ४.५.६.७.९
७.काठ.सं.६.२
अतः ऐसा कहा जा सकता है कि जो अन्तरिक्ष आत्मा की आन्तरिक शक्ति माना गया है उसके मूल रूप की संज्ञा "उरु अंतरिक्ष” है जो अनेक अन्तरिक्षाणि हो कर नानात्व में प्रकट हो जाती है और इन अन्तरिक्षों को ही पूर्वोक्त दैवीत्रिलोकी और मानुषीत्रिलोकी में विभक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रसंग में एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि मानुषीत्रिलोकी के जो नाम सामान्यतः क्रमशः द्यौ, पृथिवी और अन्तरिक्ष माने जाते हैं उनका क्रम कभी पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्यौ के रूप में मिलता है और कभी द्यौ, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी के रूप में। उदाहरण के लिए साधना की दृष्टि से जब साधक आरोहण करता है तो स्पष्टतः वह पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ पर आरोहण करता हुआ ऊपर "स्वः” ज्योति तक पहुंचता है। इसी प्रकार यजुर्वेद ५.१३ में साधक क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ को दृढ करने के लिए प्रार्थना करता है परन्तु अन्यत्र ऐसे भी स्थल हैं जहा क्रम उलट दिया गया है और द्यौ तथा अन्तरिक्ष के बाद पृथिवी का स्थान होता है। इस क्रम-भेद का कारण यह है कि जब साधक अपनी साधना द्वारा आरोहण करना चाहता है उस समय वह अहंकार-रूप-वृत्र पीड़ित द्यावापृथिवी को एकजुट हुआ पाता है जिसमें अन्तरिक्ष सर्वथा विलुप्त सा लगता है। परन्तु अपने तप के द्वारा वह जब ऋत और सत्य को उद्भूत करता है तो उसके परिणामस्वरूप एक नई आध्यात्मिक सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है और अन्ततोगत्वा वह पहले के समान यथापूर्व द्यौ और पृथिवी को पृथक् पृथक् ही नहीं, अपितु उनके साथ अन्तरिक्ष तथा स्वः नामक ज्योति को भी प्राप्त करता है जैसा कि अघमर्षण सूक्त के अन्त में कहा गया है।१
---
१.सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वं अकल्पयत्।
दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षम् अथो स्वः।।
इसी कारण प्रायः द्यौ और पृथिवी को दृढ़ करने तथा उन दोनों को अन्तरिक्ष से पूरित करने की प्रार्थना की जाती है१ क्योंकि साधना से पूर्व अन्तरिक्ष की क्षति हो जाने के कारण ही द्यावापृथिवी रोदसी संज्ञा ग्रहण करते हैं और मन-रूप प्रजापति को रुलाते रहते हैं । इसलिए अनेक स्थलों पर रोदसी को अन्तरिक्ष से परिपूर्ण करने की प्रार्थना की गई है।२ इन्द्र रोदसी को उषा के समान जब आपूरित करने वाला कहा जाता है तो भी निस्संदेह अभिप्राय "उरु अन्तरिक्ष” की ज्योति से ही भरपूर करने से ही होता है। इसी प्रकार जब सरस्वती पार्थिव लोकों को "उरु रजः अन्तरिक्षम् " से आपूरित करने वाली कही गई है तो उसका तात्पर्य यही होगा कि पूर्वोक्त वाक् शक्ति दिव्य ज्योति से सभी लोकों को भरपूर कर देती है।
----
१.यजुर्वेद ५.२७; ५.४३; ६.२
२.ऋ १०.१३९.२
३.ऋ ६.६१.११